National Judicial Technology Council क्या न्यायपालिका के अमृत काल का उदयाचल है?
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
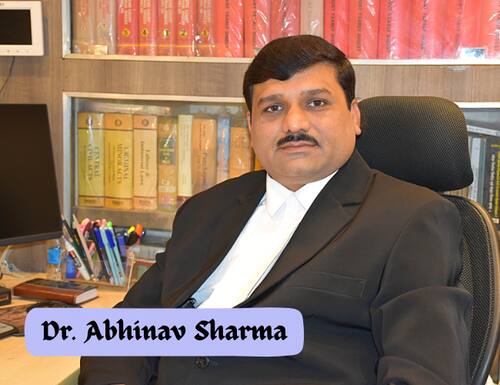
नई दिल्ली: एक अरसा हुआ जब किसी बैंक में ट्रेलर बैंकिंग के लिए आपने किस को लाइन में लगा देखा हो या शायद आप खुद बैंक गए हो, सड़क किनारे जबलपुर में कचहरी से काम निपटाकर या अनायास टहलते हुए गंजीपुरा में कचोरी चाट के साथ सुन्दर बैंड के वादन का आनंद लेते हुए या मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट के पास किसी सैंडविच या वडा पाव की दुकान पर या सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में एक अधिवक्ता के रूप में समय बिताते हुए नगद भुगतान किया हो.
कल तक यूपीआई से डरने वाला एक आम कम शिक्षित नागरिक भी अब आसानी से डिजिटल भुगतान स्वीकार्य है लिखकर खड़ा है. पहले हर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर "एक मिनट रुकिए" कहने वाला व्यापारी अब पूछता भी नहीं की पेमेंट हुआ या नहीं क्योंकि विश्वास है की पेमेंट आएगा ही, सिस्टम सील प्रूफ है. जहाँ अधिकांश यूरोपीय देश आज भी हाइवे पर टोल का नगद आहरण कर रहे है जबकि वहां सड़को की गुणवत्ता भारत से बदत्तर है और टोल मनमाना, वही भारत में हाईवे के बढ़ते सुदृढ़ जाल पर वाहन चलाने के लिए फ़ास्ट टैग का इस्तेमाल हो रहा हैं. यही भारत का अमृतकाल है, और इस सब को होने में कुछ ही वर्ष लगे.
देश ने आर्थिक डिजिटल क्रांति को सहर्ष और एक सामान्य दिनचर्या की तरह स्वीकार कर लिया है. वर्तमान में भारत में लगभग 20 करोड़ से अधिक यूपीआई कोड जारी होने के अनुमान है, जिनसे वाणिज्यिक संव्यवहार हो रहा है और लगभग 35 करोड़ से अधिक वाहन फ़ास्ट टैग के साथ सुगम और त्वरित यात्रा के गवाह बन रहे हैं,जो की डिजिटल क्रांति की एक बानगी भर है.
Also Read
- 5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
- राम मंदिर, न्यायपालिका में अपर कास्ट और राजनीतिक प्रभाव... पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने नए इंटरव्यू में सभी जबाव दिए
- पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
डिजिटल क्रांति के अमृतकाल में जहाँ देश का हर वर्ग डिजिटल क्रान्ति से जुड़ा है वहीं देश की न्यायपालिका भी अछूती नहीं है. लाखो वर्ग किलोमीटर में फैले भारत गणराज्य के 3459 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगभग 22000 अधीनस्थ न्यायालय है, जिनमे लगभग 740 ज़िला संवर्ग न्यायालयो सहित 25 हाईकोर्ट और एक सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ देश में एक बेहद बड़ा न्यायिक तंत्र भी काम कर रहा है जिसमे भी डिजिटल प्रोसेसिंग ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मध्यस्थता के लिए बनाये एस-ब्लॉक के उद्घाटन अवसर पर दिसंबर 2022 में स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही देश की न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों में तब्दील करना चाहती है और यह भविष्य भी है. उन्होंने कहा था कि देश को अब तैयार होने की जरूरत है जब हमारे देश की सम्पूर्ण न्यायपालिका जल्द ही पेपरलेस होगी.
CJI और E-कमेटी के सराहनीय कदम
वर्ष 2005 में ई-कमेटी के गठन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया की देश की सभी न्यायालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए इसके लिए धीरे धीरे ही सहीं लेकिन ठोस कदम उठाये गए और एक इंफ्रास्ट्रचर खड़ा किया गया, जो शीघ्र ही देश के न्यायिक प्रक्रिया की रूपरेखा बदलने वाला साबित होने जा रहा है.
ई कोर्ट कमेटी के चैयरमेन के रूप में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इससे एक कदम और आगे बढाते हुए आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के सहयोग से लाइव ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल कर इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है. संवैधानिक पीठ में एक प्रकरण की सुनवाई में इसका न्यायिक प्रक्रिया में प्रायोगिक उपयोग हुआ ताकि इस तकनीक की व्यावहारिकता और गुणावगुण पर अध्ययन किया जा सके. इतना ही नहीं मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर वर्षो से धूल खा रही सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स नामक पत्रिका जिसमे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय प्रकाशित होते थे का भी डिजिटल संस्करण ई-एससीआर के नाम से सभी न्यायालयों की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है.
ई-एससीआर का डाटा बेस वर्तमान में भले ही 34000 निर्णयों का है, और कम है, लेकिन जल्द ही इस पर तेजी से काम किया जा सकता है और विस्तृत रूप देने की कवायद की भी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाईकोर्ट के आदेशों की अधिकारिक स्थानीय भाषा में रूपान्तरित प्रतियाँ भी अब इस व्यवस्था से उपलब्ध है और इस पर तेजी से काम चल रहा है जिसमे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और लॉ रिसर्चर की कई टीम काम कर रही है. देश की न्यायपालिका के लिए यह एक नया प्रयोग है.
देश की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और तकनीक से सम्बल लेकर मुकदमों के तीव्र निस्तारण के लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट भी अब नया हथियार बन रहा है.आम जनता के साथ साथ देश के दूरस्थ हिस्सों में कार्यरत वकीलों, विधि छात्रों को कोर्ट प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों से अवगत करवाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
न्यायिक क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के तहत एक इकोसिस्टम बनकर लगभग तैयार है जिसके दो चरणों का काम पूरा हो चुका है तथा तीसरे चरण की ओर अग्रसर है. इस पर खर्च के लिए 639. 411 करोड़ रुपये प्रथम चरण में और 1670 करोड़ रुपये द्वितीय चरण में बजट प्रावधान किये गए है. वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के अमृत काल को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपए की मंजूरी अंतिम रूप में है, इसके लिए तीसरे चरण का नीति ड्राफ्ट बनाकर अनुमोदन के लिए तैयार किया जा चुका है.
न्याय आपके द्वार
जहाँ पूर्व में "न्याय आपके द्वार", "सुगम न्याय" जैसे वाक्य केवल कथानक थे और आमजन को न्याय तक पहुंच सिमित ही थी वही यह दायरा डिजिटल इंडिया की क्रांति के बाद बेहद तेजी से बढ़ा है और अब न्यायपालिका की ना केवल कार्यप्रणाली का सीधा प्रसारण ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है, बल्कि न्यायिक आदेश और निस्तारण की गति पर दिन प्रतिदिन नियंत्रण के लिए एक न्यायिक काउंट डाउन मीटर भी ऑनलाइन नेशनल जुडिशयल डाटा ग्रिड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो चुका है.
NJDG पर देश के लंबित और निर्णीत 20.86 करोड़ मुकदमों की सूचना सहित 18.02 करोड़ न्यायिक निर्णय उपलब्ध है जिन्हे कोई देख और डाउनलोड कर सकता है.
ई-कमेटी और एनआईसी द्वारा विकसित देश के केंद्रीकृत सूचना सिस्टम (सीआईएस) द्वारा अधीनस्थ अदालतों में प्रतिदिन अधिवक्ता और याचिकर्ताओं सहित आरोपीगण को प्रकरण की अद्यतन सूचना प्रतिदिन अपडेट की जाती है, अधिवक्तागण और एक याचिकाकर्ता स्वयं भी ई-कोर्ट के मोबाइल एप्लिकेशन से प्रतिदिन अपने मुकदमो पर नजर रख सकता है. मुकदमों को सूचीबद्ध करने और उनके समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए केस फ्लो मैनेजमेंट की एक पद्धति विकसित की जा रही है, लेकिन इसमें कई मुश्किलें भी है.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 3,80,047 ईमेल और 3,51,501 मोबाइल एसएमएस देश की न्यायपालिका द्वारा अधिवक्ता और पक्षकारो को किये जाते है. जुलाई 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 7.94 करोड़ से अधिक ईमेल और 7.34 करोड़ से अधिक प्रतिदिन एसएमएस अब तक इस सीआईएस सिस्टम से किये जा चुके है और घर बैठे ही पक्षकरो को उनके प्रकरणों की प्रगति की पूरी जानकारी दी जा रही है. देश के सभी हाईकोर्ट में निर्णीत हो चुके और पेश हो रहे या लंबित पड़े सभी मुकदमों के सम्पूर्ण रिकार्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है.
अमृत काल की प्रगति धीमी क्यों?
देश की न्यायपालिका में नए प्रयासों के बावजूद क्या इसे न्यायपालिका का अमृत काल कहा जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक तो है लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जिस प्रकार डिजिटल पेमेंट और टोल पर फ़ास्ट टैग को त्वरित गति से स्वीकार किया गया और देश ने उसे जीन की शैली बना लिया है उसकी अपेक्षा न्यायापालिका में तकनीक से होने वाली प्रगति की गति अत्यंत धीमी है और ई-कमेटी व भारत सरकार के सकरात्मक सहयोग के बाजवजूद अधिकाँश प्रयास कागजों से आगे बढ़ने में समय ले रहे है. इस सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों का विश्लेषण कर तीसरे चरण की रूप रेखा बनाई जा चुकी है.
कुछ बाते फिर भी गौर करने वाली है जो की चुनौतियों के रूप में सामने है. सबसे पहले तो यह कि देश की विविधता और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अभी हर राज्य के हाईकोर्ट में विभिन्न वर्ग में मुकदमों का वर्गीकरण होता है जिस कारण प्रत्येक हाईकोर्ट में मुकदमों को बांटने, सूचीबद्ध करने, निस्तारित करने, आदि की अपनी अलग अलग वर्गीकृत व्यवस्था है. देश के इन हाईकोर्ट में जब तक एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक अदालतों में तकनीक के इस्तेमाल से सफलता के कीर्तिमान पर निशाना लगाना आसान नहीं होगा.
न्यायिक रूप से तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कहे जा सकते है लेकिन संवैधानिक रूप से प्रत्येक हाईकोर्ट दैनिक कार्यकलाप के लिए अपने अलग नियम क़ानून बनाने को स्वतंत्र है और यह सम्बंधित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर निर्भर है की वह अपने हाईकोर्ट में किस प्रकार की डिजिटलिकरण की नीति लागू करते है. हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में अपनी चिंता तक जाहीर कर चुके है. राह लम्बी अवश्य है लेकिन मंजिल दूर नहीं है, अमृत कल के उदयाचल पर नए सूर्य का उदय स्पष्ट दिख रहा है लेकिन यह भी समझना जरूरी है की तकनीक जब तक रोजमर्रा की जरूरत नहीं बनेगी उसमें किए जाने वाले प्रयासों से अपेक्षित सफलता हासिल नहीं होगी.
नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (NCMS)
अदालतों में मुकदमों को सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रक्रिया सभी अदालतों में एक समान होना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या इस समय हाईकोर्ट की प्रणाली से है जहां मुकदमों को सूचिबद्ध करवाना और सूचीबद्ध होने के बाद सुनवाई करवा पाना एक चुनौती बना हुआ है. अधिकांश हाईकोर्ट में नियम दशकों पुराने है, दिल्ली, केरल जैसे कुछ हाईकोर्ट तकनीक का बेहद उम्दा इस्तेमाल कर रहे है वहीं अन्य हाईकोर्ट में तकनीक केवल केन्द्रीकृत सीआईएस सिस्टम तक ही सीमित है और पेपरलेस हाईकोर्ट अभी धरातल पाने को जमीन तलाश रहे है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस सब में एक राष्ट्रव्यापी मिसाल है जहाँ तकनीक का अभूतपूर्व इस्तेमाल कर देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया है.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस ए एम खानविलकर, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, ने केंद्र सरकार को एक नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी थी जिसे विधि मंत्रालय ने स्वीकृत भी किया. लेकिन कानूनी उलझनों के चलते यह एक राष्ट्रव्यापी सिस्टम बनाने के बजाय प्रशासनिक दृष्टि से हाईकोर्ट को मार्गदर्शन देने वाली कमेटी मात्र बन कर रह गयी है. तथापि मध्यप्रदेश ने इसके लिए अथक प्रयास कर रजिस्ट्रार (आई टी ), रजिस्ट्रार (नेटवर्क कम्युनिकेशन) और रजिस्ट्रार (सिस्टम इंजीनियरिंग) जैसे पद सृजन कर विशेषज्ञ लोगों को नियुक्त कर एक ऐसी वेबसाइट और केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसने अधिकांश कर्मचारियों की सेवाओं को सरप्लस कर दिया. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुक़दमे की फाईल का मूवमेंट लगभग समाप्त कर दिया और कम्प्यूटर आधारित मुकदमों के सूचीबद्ध किये जाने की प्रक्रिया बना दी जिससे मुकदमें स्वतः ही सूचीबद्ध होने शुरू हुए.
अधिवक्ताओं को कोर्ट ऑफिसर मानते हुए उनके छुट्टी पर होने पर उनके सभी मुक़दमे डीलिस्ट कर आगामी तरीको पर लगाने का प्रावधान किया गया है. इस प्रकार मुकदमों की लिस्टिंग के लिए एक सुदृढ प्रक्रिया बनाई गई है जो कारगर हुई है और अनुकरणीय है. केस फ्लो मैनेजमेंट के मध्य प्रदेश मॉडल का अध्ययन भी अन्य राज्य के हाईकोर्ट कर रहें है, लेकिन मुख्य न्यायाधीशों के रिटायरमेंट, तबादले और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के चलते अधिकांश जगह मॉडल मूर्त रूप नहीं ले सके.
हालांकि, अब ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए तैयार किये गए डिजिटल कोर्ट एवं रोड मैप के ड्राफ्ट प्रारूप में इसकी झलक साफ़ दिखाई दे रही है जिससे पूरे देश में नई उम्मीद पैदा हुई है. वर्तमान में वकील और पक्षकार दोनों के सामने मुकदमे सूचीबद्ध करना एक चुनौती है.
पेपरलैस डिजिटल कोर्ट - ई-कोर्ट
देश में तकनीक के इस अमृत काल के उदय को इस बात से पहचाना जा सकता है कि देशभर की हाईकोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच को देश की पहली पेपरलैस बेंच होने का खिताब मिला है वहीँ देश का पहला जिला स्तरीय पेपरलैस कोर्ट कड़कडूम दिल्ली में 8 फरवरी 2010 को स्थापित किया गया था.
उड़ीसा हाईकोर्ट ने सितम्बर 2022 में 30 जिला अदालतों में पेपरलैस कोर्ट का अनावरण किया. इसी तरह से देश के अन्य राज्यों में भी पेपरलेस अदालतों की कवायद जारी है. इसके बावजूद मध्यप्रदेश इसमें भी काफी आगे है जहाँ अधीनस्थ अदालतों में नोटिस जारी करने, समन आदि की तामील के लिए भी इ-कोर्ट सिस्टम ही उपयोग किया जा रहा है.
वही सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली हाईकोर्ट और हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने भी इस दिशा में एक नई पहल की है जहाँ अब मुक़दमे पूर्ण रूप से डिजिटली पेश किये जा सकते है. यहां तक कि जज भी बिना फिजिकल फ़ाइल के कंप्यूटर पर ही फाइल पढ़ सकते है और किसी भी मुक़दमे को तत्काल सूचीबद्ध कर उस पर सुनवाई कर सकते है. जिसके चलते पुराने समय की तरह फाइल के फिजिकल मूवमेंट को लगभग समाप्त सा कर दिया है.
ऐसा नहीं की देश के अन्य हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग की प्रक्रिया नहीं है. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में एक ही लॉगिन आईडी से अधिवक्ता या निजी व्यक्ति किसी भी हाईकोर्ट या अधीनस्थ अदालत में ई-फाइलिंग कर सकते है. लेकिन अधिकांश हाईकोर्ट में ई फाइलिंग के साथ साथ कागजी फाइल भी पेश किये जाने के चलते पेपरलेस कोर्ट की रूपरेखा मूर्त रूप नहीं ले पा रही.
राजस्थान हाईकोर्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है जहाँ जमानत याचिकाओं की पेपरलेस सुनवाई की प्रक्रिया तो उपलब्ध है और यह कैसे काम करती है इसका विस्तृत उल्लेख भी सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी की वेबसाइट पर तो मिलता है लेकिन धरातल पर इसका उपयोग नहीं हो रहा, जिसके चलते राजस्थान हाई कोर्ट पेपरलेस अदालत के रिकॉर्ड का भाग बन कर रह गया है. देश के हाईकोर्ट में ऐसे अन्य कई उदाहरण है. इस का प्रमुख कारण है की इस तकनीक के विकास की प्रक्रिया से वकील और न्यायालय पूरी तरह आत्मसात नहीं हुए है और वर्षो से चली आ रही फाइलों के माध्यम से सुनवाई को सहज मानकर उसी पर निर्भरता बरकरार है.
ई -फाइलिंग का भी यही हाल है जबकि ई -फाइलिंग के लिए वर्ष 2019 में केंद्रीय विधि मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट फी, शुल्क, स्टाम्प आदि के भुगतान के लिए ई पोर्टल तक बनाया जा चुका है जिसमे आम जनता और वकीलों को डिजिटल स्टाम्प या कोर्ट फीस के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. इस मामले में केंद्र सरकार हर संभव सहायता और इंफ्रास्ट्रक्टर मुहैया करवा रही है लेकिन राज्य स्तरों पर स्थानीय सरकारों को भी प्रयास करने होंगे ताकि हाईकोर्ट भी शीघ्र पेपरलेस हो सके.
कोरोना काल बनाम अमृत काल
कोरोना काल में लॉक्डाउन के दौरान देश में न्यायिक प्रक्रिया पर भी गहरी मार पड़ी थी लेकिन इस पर भी डिजिटल क्रांति का अमृत काल ही हावी हुआ और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट कमेटी द्वारा तत्समय तक विकसित की जा चुकी ई-फाइलिंग, ई-कोर्ट फीस और वर्चुअल हियरिंग व्यवस्था के चलते पूरे देश ने न्यायपालिका के अलग स्वरूप की अनुभूति की. यह कहा जा सकता है कि देश की न्यायपालिका ने एक आपदा को अवसर के रूप में तब्दील कर दिया.
कोविड के दौरान देश के अधिकांश अदालत पेपरलेस मोड में काम कर रही थी, स्कैन फाइलों को देख कर अदालतें फैसले कर रही थी. लेकिन कोरोना काल के अंत के साथ ही विधिक पेचीदगियों से भरी मुकदमा पेश करने की व्यवस्था फिर से हिस्सा बन गयी. अधिकांश हाईकोर्ट और अदालतें पुनः पूर्वर्ती अवस्था में आ गयी हलाकि कई हाईकोर्ट ने सीख लेते हुए कार्यवाही की और न्यायिक प्रक्रिया की सुनवाई की लाइव प्रोसीडिंग्स तक की अनुमति दी.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जहाँ 7 अक्टूबर 2021 को इस दिशा में नियम बनाए वही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 13 जनवरी 2023 को नियमों का गजट प्रकाशन किया. वर्तमान में देश के 25 हाईकोर्ट में से केवल 6 हाईकोर्ट में मुकदमों की लाइव सुनवाई केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है, जिसमे गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और पटना उच्च हाईकोर्ट शामिल है. फिलहाल देश के कई हिस्सों में ट्रैफिक चालान भुगतने के लिए वर्चुअल कोर्ट भी अस्तित्व में आ गए है जिसमें बिना अदालत जाये भुगतान किया जा सकता है.
एनजीटीसी के गठन का प्रस्ताव
देश के हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का कोई संवैधानिक प्रशासनिक नियंत्रण न होने और एकीकृत प्रयासों की कमी सहित स्थानीय विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए ई-कोर्ट के तीसरे चरण की श्रेणी में एक राष्ट्रीय स्तर की जुडिशल काउंसिल के गठन का प्रस्ताव किया गया है. जिसे एक कानून बनाकर विधिक संस्था बनाना प्रस्तावित है जो की भविष्य की डिजिटल न्यायपालिका के स्वरूप को मूर्त रूप देगी. भी तक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के सहयोग से अन्य तकनीकी व्यक्तियों को शामिल कर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट की कमेटियां डिजिटल न्यायपालिका का स्वरूप देने में लगी है.
प्रस्तावित एनजीटीसी में न्यायपालिका, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञों का एक बोर्ड इस पर काम करेगा ताकि देश की सम्पूर्ण न्यायपालिका जल्द से जल्द पेपरलेस हो, मुकदमों को सही समय पर और बिना विलम्ब सूचीबद्ध कर निस्तारित किया जा सके और यह सब बहुत जल्द और तेजी से होने वाला है.
यह तो स्पष्ट है की देश की न्यायिक व्यवस्था तेजी से करवट बदल रही है। उच्चतम न्यायालय भी प्रयासरत्त है और केंद्र की सरकार कटिबद्ध, इसलिए वर्तमान समय में न्यायपालिका के उदयाचल पर अमृत काल के सूर्य के उदय होने कि झलक साफ़ देखी जा सकती है ऐसे में तकनीक से बावस्ता लोगो के न्यायपलिका में प्रवेश की ओर भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कॉलेजियम को विशेष ध्यान देना होगा. जिस प्रकार से देश में डिजिटल पेमेंट और फ़ास्ट टैग को एक जीवशैली के रूप में स्वीकार किया उसी प्रकार न्यायपालिका में भी तकनीक को जरूरत से जोड़ कर ऐसे पेश करना होगा ताकि उसकी स्वीकारोक्ति हो और आजादी से पहले से चली आ रही न्यायिक परम्पराओ की बेड़िया तोड़ने के लिए इस प्रक्रिया के भागीदार वकील और पक्षकार खुद आगे बढ़कर इसे स्वीकार करें.
पेपरलैस कोर्ट होने के साथ साथ मध्यप्रदेश मॉडल के अनुरूप मुकदमों को समयबद्ध रूप से निस्तारण के लिए सूचीबद्ध करने की केस फ्लो मैनेजमेंट व्यवस्था को लागू कर देश में न्यायपालिका जल्द ही एक बड़े बदलाव की तैयारी में है जिसमे नेशनल जुडिशल टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन भी एक भूमिका अदा कर सकता है.
