क्या है जनहित याचिका? यह कब और कैसे दायर की जाती है
हमारे आस पास अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं जिसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि पूरे समाज या शहर पर होता है. कभी कभी वो मामलें पूरे देश को प्रभावित कर जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम अदालत तब ही जा सकते हैं जब कोई अपना नुकसान हो लेकिन ऐसा नहीं है.
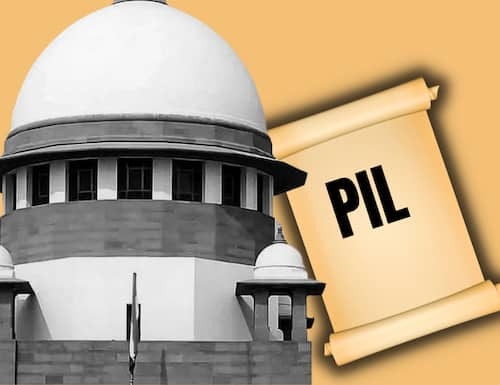
नई दिल्ली: आम जीवन में हम अदालत का दरवाजा तभी खटखटाते हैं जब हमारा कोई निजी नुकसान होता है. सोचिए उन मामलों के बारे में जिससे कुछ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय, शहर, राज्य या पूरा देश प्रभावित होता है. क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों को लेकर किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है. आपने सुना जरूर होगा कि किसी ने कोई जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) दायर की है उच्च या उच्चतम न्यायालय में. इस तरह मामलों को क़ानूनी तरीके से सामने जनहित याचिका द्वारा किया जाता है. आईए जानते हैं क्या है जनहित याचिका और इसे कैसे दायर किया जाता है.
क्या है जनहित याचिका?
आपने अब तक समझ लिया होगा कि यह याचिका "जन" यानि लोगों के हित से जुडी है. यह मुकदमेबाजी (Litigation) का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है. इसे लोगों के अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग कह सकते है.
जनहित याचिका की अवधारणा को अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है. हमारे देश के कानून के अनुसार PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना होता है. यह याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि खुद अदालत या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है. इसे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई एक शक्ति या ताकत कहा जा सकता है.
Also Read
- CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी
- दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत
- बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
कई बार लोगों को लगता है कि जनहित याचिका, रिट याचिका की तरह है लेकिन ऐसा नहीं है रिट याचिका अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका "आम जनता के लाभ" के लिये दायर की जाती है.
जनहित याचिका की अवधारणा हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके.
जनहित याचिका की शुरुआत
जनहित याचिका आने से पूर्व कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता था जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो. साल 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया. 1979 में अदालत ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला किया जिसे पीड़ित ने नहीं बल्कि उनकी ओर से किसी दूसरों ने मामले को दाखिल किया था. 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों को लेकर एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया था कि उन्हें सजा भी दी गई होती तो उतनी अवधि की नहीं होती जितनी उन्होंने विचाराधीन होते हुए काट ली हैं.
इस खबर को ही आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की. सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला और यह याचिका "जनहित याचिका" के रूप में प्रसिद्ध हुई. इस तरह से 1979 से इसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय ने की. बाद में इसी प्रकार के अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया.
जनहित याचिका दायर करने का क्षेत्र
हर मामले को जनहित याचिका में तहत दायर नहीं किया जा सकता है. आप उन्ही मामलों को जनहित याचिका के तहत दायर कर सकते हैं जो मामला या मुद्दा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करता है, जैसे; प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि.
जनहित याचिका का महत्व
.समाज में बदलाव करने का एक बेहतरीन साधन है.
.कानून के शासन को बनाए रखने में भी यह मददगार है.
.कानून और न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने में भी एक अहम भूमिका अदा करता है.
.जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य ही है गरीबों और हाशिये के वर्ग के लोगों के लिये न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना. यह सभी के लिये न्याय की सुलभता का लोकतंत्रीकरण है.
कौन दायर कर सकता है जनहित याचिका
जनहित याचिका को किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसा समूह, या गैर सरकारी संगठन के द्वारा दायर किया जा सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि ये कोई पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है. इसे कोई भी देश का नागरिक दायर कर सकता है केवल एक ही शर्त है कि इसमें कोई निजी लाभ नहीं होना चाहिए. यह जनहित में होनी चाहिए.
अगर मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो अदालत स्वत: संज्ञान भी ले सकती है.
कहां दर्ज कर सकते हैं जनहित याचिका
जनहित याचिका रिट याचिका (Writ Petition) का विस्तार है. इस याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है. आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के समक्ष और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर कर सकते हैं.
अगर आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको जनहित याचिका की पांच प्रतियां (copy) जमा करनी होंगी. जनहित याचिका की प्रति प्रतिवादियों को तभी दी जाएगी जब अदालत उसके संबंध में नोटिस जारी करेगी.
अगर आप हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको उसकी दो प्रतियां जमा करनी होगी. साथ ही आपको अग्रिम रूप से उसकी कॉपी को उत्तरदाताओं को देनी होगी.
कैसे दायर करें जनहित
जानकारी के अभाव में लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि जनहित याचिका को दायर करना बहुत कठिन है लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप चाहें तो कोई साधारण पत्र और पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष अपना मुद्दा रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर माना जाता की पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए इस याचिका को दायर करने के लिए.
जनहित याचिका के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स अपनाने होंगे:
.जनहित याचिका को दायर करने से पहले किसी अनुभवी जनहित याचिका अधिवक्ता से संपर्क करें, ताकि आपका बेवजह वक्त बर्बाद ना हो. अगर आप चाहते हैं कि खुद याचिका दर्ज करें तो वह भी कर सकते हैं.
. जनहित याचिका से संबंधित दस्तावेजों का मिलान सुनिश्चित करें.
. तय करें कि आपको याचिका किस कोर्ट में दायर करनी है.
. अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहें तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित करते हुए याचिका दायर करें.
. वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर कर रहें तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए याचिका दायर करें.
जनहित याचिका दायर करने का शुल्क
मुकदमे के लिए शुल्क केवल 50 रुपये प्रति प्रतिवादी है जिसका उल्लेख जनहित याचिका में किया गया है और इसका उल्लेख याचिका में भी किया जाना चाहिए हालांकि, पूरी कार्यवाही की कुल लागत याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील पर निर्भर करता है.
जनहित याचिका दायर करने के लिए जरूरी दस्तावेज
.याचिकाकर्ता को अपना नाम, डाक का पता (Postal Address), ई- मेल, फोन नंबर, पेशा, वार्षिक आय और पैन नंबर देना होगा.
. सभी पीड़ित पक्षों का नाम और पता.
.उन सरकारी एजेंसियों या अन्य के नाम और पते की सूची बनाएं जिनसे राहत मांगी गई है.
.अधिकारों के उल्लंघन को जन्म देने वाले तथ्यों की सूची बनाएं जिनका सामना किया जा रहा है.
. किस तरह का उल्लंघन या चोट पहुंचाया जा रहा है.
. किसी तरह का कोई निजी लाभ हो ये भी आपको बताना होगा.
. याचिकाकर्ता को इस बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए कि यदि अदालत कोई शुल्क लगती है तो क्या वे लागत का भुगतान करने में सक्षम होंगे
इन मामलों में आप जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं
.सेवा से संबंधित मामला
.ग्रेच्युटी, पेंशन, वेतन आदि से संबंधित मामले
.मकान मालिक किरायेदार मामले
.सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध मुद्दों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें.
.किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला का मुद्दा.
.उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में जल्द सुनवाई के लिए आग्रह करने वाली याचिका.
