क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
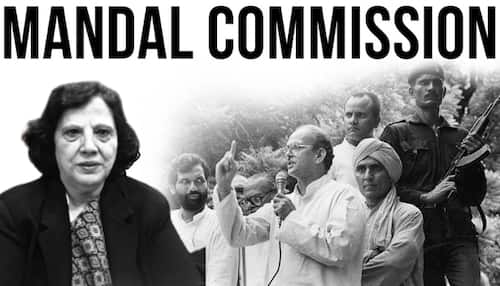
नई दिल्ली: भारतीय संविधान की यात्रा में कई ऐसे मामले सामने आये जिनके द्वारा आमजन की समस्याएं तो उजागर हुई ही अपितु उनका समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया. इन्ही में से एक था, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (1992) का मामला जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है.
यह 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
क्या था ममाला
हमारे संविधान में सामाजिक और शैक्षिणिक पिछड़ेपन को मान्यता दी गई है, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी (Other Backward Classes) के लिए अलग आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन इन्हें "क्रीमी लेयर" (पिछड़े वर्ग का एक निश्चित आय से ऊपर का अगड़ा वर्ग) से बाहर कर दिया, साथ ही ये निर्देश दिया कि किसी भी समय आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
Also Read
- Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
- बच्चे को चूमने का मामला: दलाई लामा पर चले POCSO का मुकदमा, दिल्ली HC ने ये कहकर PIL की खारिज
- Ram Mandir Inauguration: प्राण-प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग, Allahabad HC में याचिका दायर
इस बहस की शुरुआत 1980 में हुई, जब बीपी मंडल की अध्यक्षता वाली दूसरी पिछड़ा वर्ग समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है।
हालाँकि, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया गया।
मंडल आयोग
चूकि इस आयोग की अध्यक्षता सांसद (MP) Bindheshwari Prasad Mandal ने की थी, इसलिए इसे मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है. इस आयोग को 1 जनवरी, 1979 को स्थापित किया गया था, जिसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की अनुशंषा की जानी थी।
आयोग द्वारा सिफारिश की गई की OBC को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये, उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर पदोन्नति में समान 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये, आरक्षित कोटा यदि पूरा नहीं किया गया है तो इसे 3 वर्ष की अवधि के लिये आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
साथ ही, आयोग ने कहा की OBC को SC और ST के समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, सरकारी अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये, तथा सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाये।
मंडल आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा और जब सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया तो जहाँ छात्रों ने विरोध में आत्मदाह किया।वहीं दूसरी ओर इसे इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती मिली .
याचिकाकर्ता इंदिरा साहनी ने तीन प्रमुख तर्क दिए
1- आरक्षण के विस्तार ने अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया है
2- जाति पिछड़ेपन का विश्वसनीय संकेतक नहीं है और,
3- तीसरा सार्वजनिक संस्थानों की कार्यक्षमता ख़तरे में है
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना लेकिन कुछ शर्तों के साथ आइये जानते है उन शर्तो को-
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतिशत कैप की सीमा में ही होना चाहिये और पदोन्नति में इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। क्रीमी लेयर की अवधारणा भी न्यायालय द्वारा समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लिये पेश की गई थी।
कैरी फॉरवर्ड नियम (जिसके द्वारा आगामी वर्ष में अपूर्ण रिक्तियों को भरा जाता है) को 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।
सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा न कि पदोन्नति पर।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कि पृष्ठभूमि कालेलकर आयोग से ही शुरु हुई. 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो सरकार ने दलित वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को लाभ देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का इस्तेमाल किया।
हालांकि, इससे पहले देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कोई रिकॉर्ड नहीं था; ये जातियां ST और SC की तरह पिछड़ी नहीं थीं। 29 जनवरी, 1953 को इस मुद्दे के समाधान के लिए भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (First OBC Commission) का गठन किया गया।
काका कालेलकर को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और बाद में इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना गया। इसके बाद आरक्षण से संबंधित कई मामले सामने आये जिसने वंचितों के अधिकार के लिए इस मंडल आयोग कि रिपोर्ट का विरोध किया।
बालाजी बनाम मैसूर राज्य का मामला
इस मामले में न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा समाज के शेष वर्गों के हितों में कटौती करके नहीं किया जाना चाहिए।
यहां बता दे की संविधानं के अनुच्छेद 15(4) के साथ-साथ 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को प्रदत्त शक्तियां कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रदत्त हैं ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके।
देवदासन बनाम भारत संघ, जिसे 'कैरी फॉरवर्ड रूल केस' के रूप में भी जाना जाता है, में अनुच्छेद 16(4) के दायरे पर विचार किया गया और इस मामले में सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिगामी वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सरकार के "प्रवर्तन दिशानिर्देश" को शामिल किया गया था।
एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4ख) के तहत आरक्षण दिया जा सकता है.
