Anticipatory Bail: क्या गिरफ्तारी से पहले मिल सकती है आरोपी को जमानत
धारा 438(1) के अनुसार, आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अर्जी केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है. न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय विभिन्न तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं. इस जमानत का मतलब यह होता है कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोपी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करता है तो पुलिस को उसे रिहा करना ही होगा.
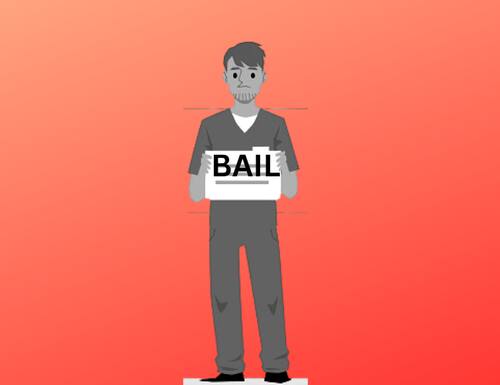
नई दिल्ली : अग्रिम जमानत का मतलब गिरफ्तारी की आशंका में जमानत पाना है. यानि पुलिस द्वारा आपके खिलाफ कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज़ की गई है और आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो इस स्तिथि में आप कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करके गिरफ्तारी से पहले ही जमानत पा सकते हैं.
हाल ही में कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामलों में अग्रिम जमानत बहुत चर्चा में भी रही है. कई मामलों में जमानत दी गई, वहीं कुछ मामलों में अग्रिम जमानत की अर्ज़ी को खारिज भी किया गया. यह इसलिए है क्योंकि अग्रिम जमानत की मांग आरोपी अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है और न्यायालय अपने विवेक के अनुसार तय करेगा कि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं.
क्या है सीआरपीसी की धारा 438
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) की धारा 438 के तहत उन मामलों में जमानत की मांग की जा सकती है, जहां आरोपी को उचित आशंका है कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकते है. इस धारा के अन्तर्गत दी जाने वाली जमानत को “अग्रिम जमानत” कहा जाता है.
Also Read
- AAP MLA अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ HC पहुंची Delhi Police, जानें क्या है मामला-सुनवाई के दौरान क्या हुआ
- पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के दोषी मुस्लिम शख्स को राहत, जानें क्यों Supreme Court ने फांसी की सजा बहाल करने से किया इंकार
- अगर चार्जशीट में नाम आया तो ट्रायल कोर्ट आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी कठोर कदम उठाएं... Patna HC के अग्रिम जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने बदला
धारा 438(1) के अनुसार, आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अर्जी केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है. न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय विभिन्न तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं. इस जमानत का मतलब यह होता है कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है और आरोपी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करता है तो पुलिस को उसे रिहा करना ही होगा.
जब न्यायालय अग्रिम जमानत की अर्ज़ी पर सुनवाई करता है तो निर्णय देने से पहले अभियोजन (Prosecution) पक्ष को सुनना अनिवार्य है.
आरोपी पर क्या शर्ते लगाई जा सकती हैं
1. आवेदक जब भी आवश्यक हो पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा यानी वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा.
2. आवेदक किसी भी गवाह को धमकाएगा नहीं और उसे गवाही न देने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
3. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकता है.
4. न्यायालय कोई भी अन्य शर्त लगा सकते हैं, जो उसे अनुकूल लगती हों. जैसे कि जमानत बॉन्ड (Bail Bond)/शिकायतकर्ता या गवाह से कोई संपर्क नहीं करना.
न्यायालय किन कारकों (Factors) को संज्ञान में लेंगे
सत्र और उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की अर्ज़ी की सुनवाई करते समय इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं.
· अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता.
· आरोपी के आपराधिक पूर्ववृत्ति की भी समीक्षा की जाएगी. विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि क्या आरोपी को पहले कभी गंभीर और हिंसक अपराध के लिए दोषी पाया गया है.
· यह भी देखा जाएगा कि क्या अपराधी जांच में सहयोग करेगा या नहीं.
· आरोपी द्वारा समान या अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना.
न्यायालय जब निर्णय पारित करता है तो उसे अपने निर्णय के समर्थन में कारण देना अनिवार्य है. महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साबिद हुसैन मोहम्मद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अग्रिम जमानत की अर्ज़ी स्वीकार किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है.
किन मामलों में अग्रिम जमानत आम तौर पर नहीं दी जाती है
अग्रिम जमानत देने की शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए. दुष्कर्म, हत्या, दहेज़ हत्या, गर्भपात या अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज़ किये गए मामलों में भी नहीं दी जाती है अग्रिम जमानत, लेकिन कुछ अपवाद (Exceptions) देखने को मिलते हैं.
भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण मामलों में दी जा सकती है. जब न्यायालय को ऐसा लगे कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है या उसके खिलाफ एक मामूली आरोप लगाया गया है या आरोपी द्वारा जमानत का गलत इस्तेमाल करने की संभावना बहुत कम है, तो ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है.
झूठे या गलत अपराधों में फसाये जा रहे आरोपियों के बचाव के लिए अग्रिम जमानत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असाधारण मामलों में ही अग्रिम जमानत की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए यानी जब अदालतें मानती हैं कि याचिकाकर्ता पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है. इसके अलावा, आरोपी के हितों की रक्षा के अलावा, अग्रिम जमानत एक कानूनी उपाय के रूप में आरोपी को उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से रोकती है.
