Juvenile Justice Act के तहत उस व्यक्ति का स्थानन, जिसने 18 वर्ष से कम होने पर अपराध किया था
किशोरों मे अपराधिक व्यवहार का बढ़ना समाज की अस्वस्थता का परिचय है. परन्तु किशोर अपराधी को सही देखभाल और संरक्षण देना आवश्यक है ताकि वो अपराध की राह को छोड़ के सुमार्ग का चयन करें और देश की उन्नति में सहयोग करें.
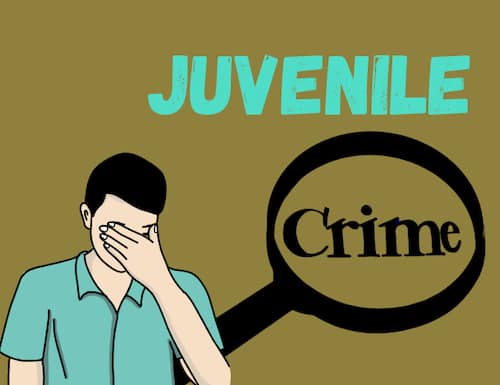
नई दिल्ली: बच्चों के पालन पोषण पर उनका पूरा भविष्य टिका होता है, यदि वो सही वातावरण से या देखभाल से वंचित रहें तो उसके अपराध की राह पर चलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं. पिछले कुछ दशकों में, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा अपराध दर में वृद्धि देखी गई है. कुछ बुनियादी कारणों में, बच्चों के पालन-पोषण का वातावरण, शिक्षा की कमी, आर्थिक स्थिति और माता-पिता की देखभाल आदि शामिल हैं. साथ ही, आजकल बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा कर उनको अपराध करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उसे आसानी से बचाया जा सके. ऐसे ही कारणों की वजह से अपराधी किशोरों के लिए किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) बनाया गया है.
दिसंबर 2012 के "निर्भया दिल्ली गैंग रेप केस", की दर्दनाक घटना के बाद कानूनी बिरादरी के बीच कानून के प्रावधानों को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसका मुख्य मुद्दा आरोपी की भागीदारी थी, जो 18 वर्ष की आयु से सिर्फ छह महीने कम था. बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में किशोर अभियुक्तों की संलिप्तता ने भारतीय विधान को एक नया कानून लाने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार, "किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015" बना. इस अधिनियम ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), 2000 को प्रतिस्थापित किया, ताकि जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सके.
किशोर न्याय अधिनियम क्या है
Juvenile Justice Act, 1986 उपेक्षित या अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है.
Also Read
- Juvenile Justice Act के तहत स्कूल 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' के आधार पर सही उम्र का फैसला नहीं किया जा सकता: Supreme Court
- Kerala Court ने नाबालिग चचेरी बहन के बलात्कारी भाई को 135 साल की सुनाई सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं ले सकते बच्चा गोद, JJ Act में निर्धारित निर्देशों का सख्ती से करें पालन: Odisha HC
यह अधिनियम कानून के साथ संघर्ष में पाए जाने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटान में एक बाल-सुलभ दृष्टिकोण अपनाना और प्रदान की गई प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए, कानून ने विभिन्न विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी की सिफारिश की.
किशोर न्याय अधिनियम की धारा-6
धारा-6 यह परिभाषित करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध तब किया हो जब वह अठारह वर्ष से कम आयु का था, तो किशोर न्याय प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे. किशोर न्याय अधिनियम की धारा-६ के तहत, उस व्यक्ति का स्थानन, जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था-
कोई भी व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और जब वह अठारह वर्ष से कम आयु का था, अपराध करने के लिए पकड़ा गया, तो, ऐसे व्यक्ति को, इस धारा के प्रावधानों के तहत, पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में माना जाएगा.
(2) उप-धारा (1) में संदर्भित व्यक्ति, यदि बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो उसे जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के स्थान पर रखा जाएगा
(3) उप-धारा (1) में संदर्भित व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 27 भी किशोर अपराध के परीक्षण के क्षेत्राधिकार बताती है-
इस धारा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई ऐसा अपराध किया जाए जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जो उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, सोलह वर्ष से कम आयु का है, तब एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, या बाल अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के तहत विशेष रूप से सशक्त किसी भी न्यायालय द्वारा, या युवाओं अपराधी के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए प्रदान किए जाने वाले समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून द्वारा विचार किया जा सकता है.
